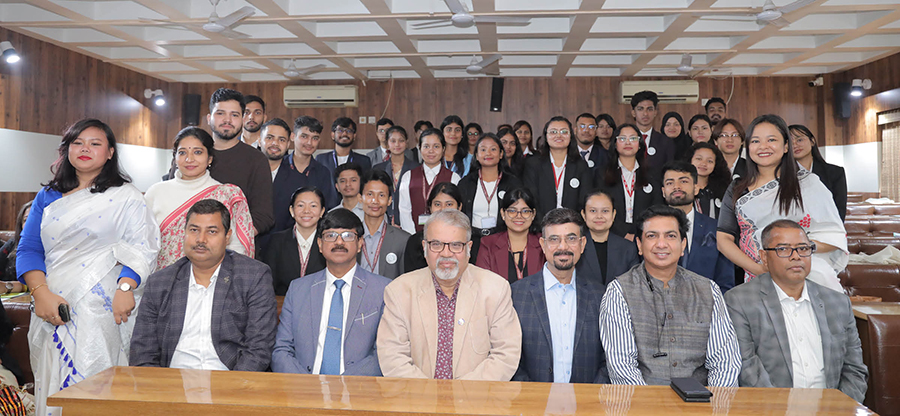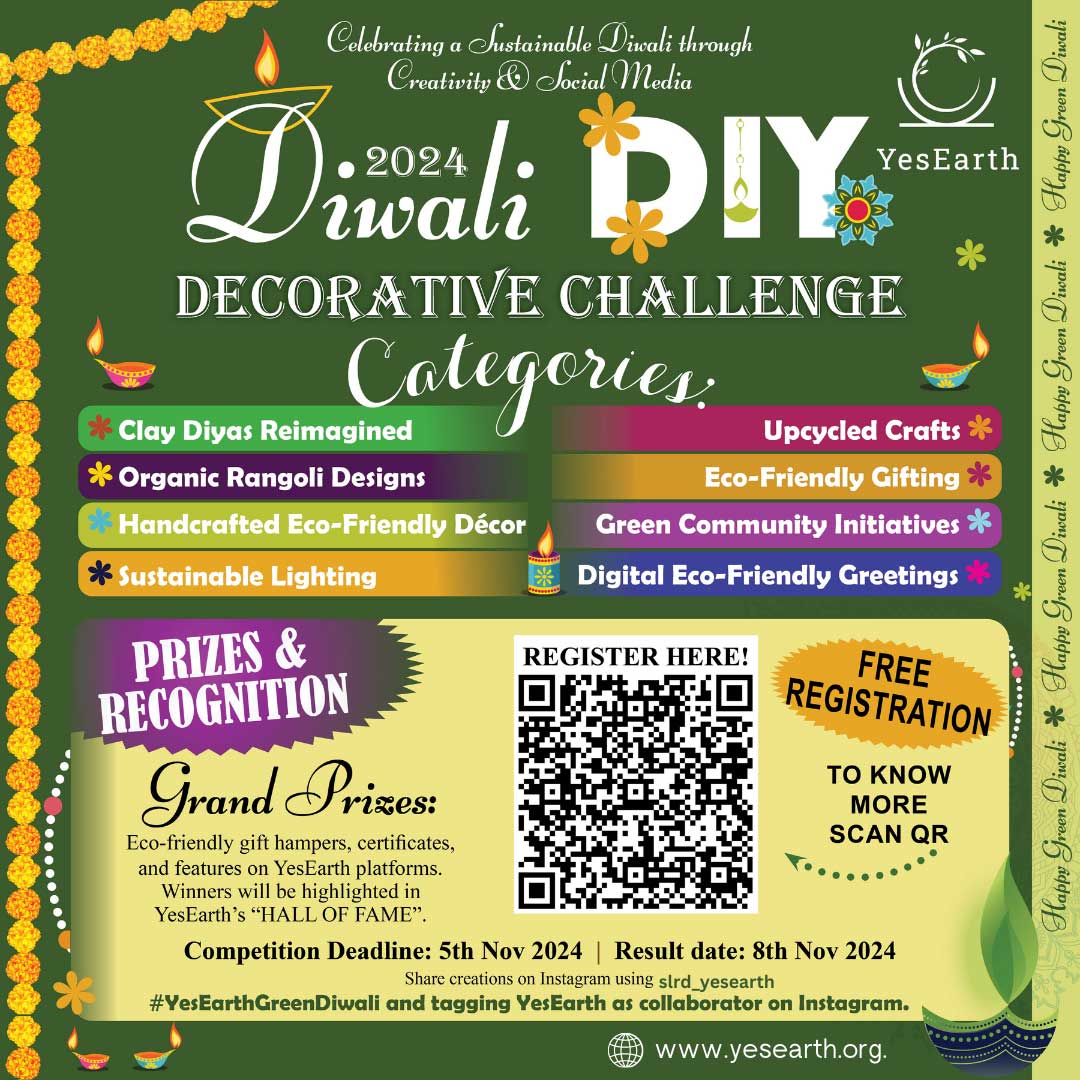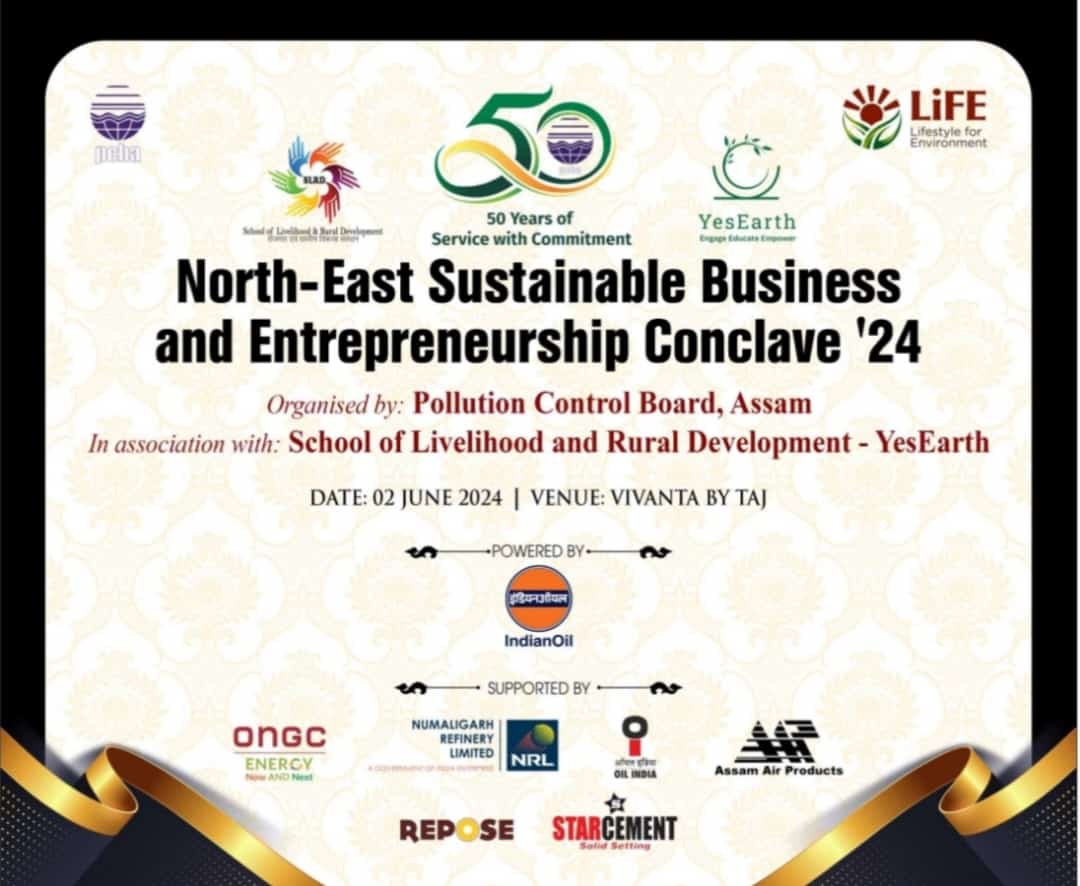उत्तर प्रदेश में कृषि वानिकी से आर्थिक लाभ : चुनौतियां तथा नवीन संभावनाएं
अनुभा श्रीवास्तव, अनीता तोमर तथा संजय सिंह
परिचयः
वनोपजों में सबसे निचले स्तर पर जलाने के लिये लकड़ी, औषधियाँ, लाख, गोंद और विविध फल इत्यादि आते हैं जिनका एकत्रण स्थानीय लोग करते हैं। उच्च स्तर के उपयोगों में इमारती लकड़ी या कागज उद्योग के लिये लकड़ी की व्यावसायिक और यांत्रिक कटाई होती है। एफ०ए०ओ० के अनुसार भारत जलावन की लकड़ी का विश्व में सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है और यह वनों में लकड़ी के पुनस्स्थापन से पाँच गुना अधिक है। वहीं भारतीय कागज उद्योग प्रतिवर्ष 3 मिलियन टन कागज का उत्पादन करता है जिसमें कच्चा माल वनों से लकड़ी और बाँस के रूप में आता है। वानिकी के वर्तमान परिदृश्य – जनजातियों और स्थानीय लोगों के जीवन, पर्यावरणीय सुरक्षा, संसाधन संरक्षण और विविध सामाजिक राजनीतिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के परिपेक्ष्य में कृषकजन कृषि वानिकी के माध्यम से इमारती लकड़ी, फलदार वृक्ष, औषधीय पौधे तथा बांस आदि का रोपण कर आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं। काष्ठध् अकाष्ठ उत्पादों के उचित बिक्री के अवसर प्राप्त करना कृषकों लिए एक कठिन चुनौती है। भारत में वानिकी एक प्रमुख ग्रामीण आर्थिक क्रिया, जनजातीय लोगों के जीवन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू और एक ज्वलंत पर्यावरणीय और सामाजिक-राजनैतिक मुद्दा होने के साथ ही पर्यावरणीय प्रबंधन और धारणीय विकास हेतु अवसर उपलब्ध करने वाला क्षेत्र है। आर्थिक योगदान के अलावा वन संसाधनों का महत्व इसलिए भी है कि ये बहुत सी प्राकृतिक सुविधाएँ प्रदान करते हैं। हवा को शुद्ध करना और सांस लेने योग्य बनाना एक ऐसी प्राकृतिक सेवा है जो वन उपलब्ध करते हैं और जिसका कोई कृत्रिम विकल्प इतनी बड़ी जनसंख्या के लिये नहीं है। वनों के क्षय से जनजातियों और आदिवासियों का जीवन प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है और शेष लोगों का अप्रत्यक्ष रूप से क्योंकि भारत में जनजातियों की पूरी जीवन शैली वनों पर आश्रित है।
कृषि वानिकी
खेतों में अन्न उपजाने के साथ-साथ अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर आर्थिक रूप से सृदृढ़ हो सकते हैं। खेत में फसल के साथ-साथ वृक्ष लगाकर भविष्य की सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कृषि वानिकी के अन्तर्गत ऐसे वृक्षों को उगाना चाहिए जो अपेक्षाकृत तेज बढ़ने वाले हो जिससे लाभ हेतु उनसे कम समय में ही उपज प्राप्त कर सकें। खेत का पूरा उपयोग कर अधिकतम व विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। अन्न का उत्पादन बढ़ा सकते हैं व लगाए गए पेड़ को बेचकर धन प्राप्त कर सकते हैं। खेत में ही चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी, कुटीर एवं लघु उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त कर सकते हैं। खेत में ही ईंधन प्राप्त कर, गोबर को कंडा बनाकर जलाने से बचाकर खाद के रूप में प्रयोग कर धन की बचत व अधिक फसल प्राप्त कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदा, यथा-बाढ़, सूखा, अधिक वर्षा आदि से कृषि फसल को क्षति पहुँचने पर अथवा कृषि फसल अधिक होने के कारण मूल्य में कमी आने पर खेत के वृक्ष को बेचकर धन अर्जित कर सकते हैं।
उपलब्ध प्राकृतिक वनों पर जैविक दबाव कम कर सकते हैं। वृक्षारोपण में वृद्धि कर भूमि एवं जल संरक्षण कर, पर्यावरण में संतुलन स्थापित कर प्रदेश व देश के विकास में योगदान दे सकते हैं
कृषि वानिकी में रोपण हेतु सीधे तने, कम शाखाओं, विरल छत्र व शाख तराशी सहने वाली वृक्ष प्रजातियों को चयन में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
कृषि वानिकी में लम्बी जड़ों वाले वृक्षों को उगाना बहुत लाभदायक होता है। यह जड़ें भूमि में जाकर नीचे से लाभदायक पदार्थ ऊपर लाती हैं जो कृषि फसलों को फायदा पहुँचाते हैं। वृक्षों की मूसला जड़ों की बढ़त इसप्रकार हो कि वे जल से खनिज लवणों के अवशोषण व फसलों की आवश्यकता के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकें।
कृषि वानिकी के अन्तर्गत द्विदलीय बीज वाले वृक्ष उगाना अधिक लाभदायक है, क्योंकि ऐसे वृक्ष हवा से नाइट्रोजन लेकर भूमि में जमा करते हैजो कृषि फसलों के लिए लाभदायक है। कृषि वानिकी अपनानेकेमहत्वपूर्णचरण
• पौधरोपन हेतु भूमि की उपलब्धता
• बाजार में उच्च मांग वाली प्रजातियों का अध्ययन तथा उनकी विपणनविधियों की जानकारी
• उचित प्रजातियों का चयन
• उच्च गुणवत्ता के पौधे प्राप्त करना
• पौधरोपण तथा इसका रख रखाव
• वानिकी काष्ठ ६ अकाष्ठ उत्पादों का निष्कर्षण, संग्रहण, पैकेजिंग, तथा प्रक्रिया प्रक्रम संबन्धित तकनीकी जानकारी
• उत्पादों के स्व-उपयोग विक्रय अथवा वानिकी पौधों की नरसेरी स्थापित कर पौधों की बिक्री
• वानिकी अकाष्ठ उत्पादों यथा, सतावर, आवला, बेल, महुआ, सहजन आदि का मूल्य संवर्धन लघु उद्योगों के रूप में वित्तीय सहता हेतु पंजीकरण
उत्तर प्रदेश के ग्रामीणवशहरी क्षेत्रों में मुख्य प्रजातियों का वितरण ()-
स्त्रोत : वन सर्वेक्षण रिपोर्ट (2021)
| क्रमांक सं. | मुख्य प्रजाति | ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण (%) | शहरी क्षेत्रों में वितरण (%) |
| 1 | आम | 31.54 | 9.81 |
| 2 | यूकेलिप्टस | 15.86 | 8.87 |
| 3 | पापलर | 9.60 | – |
| 4 | नीम | 5.71 | 15.90 |
| 5 | कीकर | 5.30 | – |
| 6 | अमरूद | – | 3.90 |
| 7 | अर्जुन | – | 3.33 |
पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रमुख काष्ठ प्रजातियाँ – वर्तमान परिदृश्य
राष्ट्रीय वन नीति 1988 व उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति 1998 के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र का एक तिहाई क्षेत्रफल वनों से ढका रहना चाहिए, परन्तु उ०प्र०में कुल वनाच्छादित व वृक्षाच्छादित क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का 9.23 प्रतिशत ही है। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण व
औद्योगीकरण आदि ऐसे अनेक कारण हैं जिसकी वजह से बडे पैमाने परनये वन क्षेत्रों को लगाये जाने की सीमित सम्भावनाएं हैं। प्रदेश में वृक्षारोपण जन सहयोग प्राप्त करके व कृषिवानिकी को जन आन्दोलन बनाकर हीप्रदेश में वृक्षावरण का अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। मानव जीवन के अस्तित्व की रक्षा के लिए वृक्ष व वन आवश्यक हैं। प्रत्यक्ष प्रभावों में मनुष्य विभिन्न आर्थिक लाभो जैसे- चारा, जलौनी, फल, जड़ी-बूटीउद्योगो में कच्चे मालनिर्माण हेतु लकडी आदि से लाभान्वित होने के साथ-साथ आजीविका प्राप्त करता है। परोक्ष प्रभावों में वन आक्सीजन उत्सर्जन एवं जल व मृदा संरक्षण जैसे कार्य मानवता को लाभान्वित करते है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रमुख काष्ठ प्रजातियाँ यूकेलिप्टस, पापलर, शीशम, सागौन, बबूल, आंवला, बेर, खैर, शहतूत आदि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि वानिकी की मुख्य प्रजातियाँ है। इसके अतिरिक्त आम, नीम, महुआ, जामुन, पीपल, बरगद, पलाश आदि प्रजातियां बाग बगीचों, घर के आस-पास या गांव की अतिरिक्त भूमि पर पायी जाती है। प्रजातियों की उपलब्धता माँग से बहुत अधिक कम है अर्थात् मांग और आपूर्ति का अन्तर बढ़ता ही जा रहा है। ग्रामीण तथा शहरी स्तर की चारा, लकडी तथा जलौनी की मांग निरन्तर बढ़ती जा रही हैं। ग्रामीण अपनी दैनिक आवश्यताओं जैसे- जलौनी, लकड़ी की पूर्ति व्यापक स्तर पर बाजार में उपलब्ध लकडी से करते है जो विभिन्न ग्रामीण तथा शहरी बाजारों मे वनों तथा अन्य स्रोत्रों से उचित मूल्य में उपलब्ध है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि वानिकीः वृक्षारोपण की नई संभावनायें
कृषि वानिकी के अन्तर्गत खेत के चारों तरफ मेड़ों पर दो या तीन पंक्तियों में अथवा खेतों के अन्दर पंक्तियों में एक निश्चित दूरी में फसलों के साथ वृक्षों को रोपित किया जाता है। इस पद्धति में रोपित वृक्षों के मध्य दूरी इस प्रकार रखी जाती है कि उनके मध्य में कृषि फसलों को उगाया जा सके तथा कृषि कार्य हेतु उनके मध्य से ट्रेक्टर आदि चलाया जा सके।
1. राज्य वन विभाग के नियमानुसार प्रजातियों का कटान तथा दुलान समयानुसार उचित परमिट प्राप्त कर के किया जाता है। उचित दर पर वृक्ष प्रजातियों की बिक्री उपयुक्त बिक्री स्त्रोत से की जा सकती हैः वन निगम, आरा मशीन, प्लाईवुडध्वनीयर उद्योग अन्य काष्ठ उद्योग। 2. प्लाईवुडधवनीयर उद्योग में मुख्य रूप से यूकेलिप्टस तथा पापलर प्रजातियों का प्रयोग होता है। इस उद्योग में बिक्री हेतु 5-8 वर्ष की तैयार लकड़ी ही प्रयोग की जाती है। 18-50 इंच मोटाई के यूकेलिप्टस तथा पापलर के वृक्ष विनीयर उद्योग हेतु उपयुक्त होते हैं। 52 इंच के टुकड़े युकेलिप्टस तथा 40 इंच के टुकड़े पापलर हेतु उपयुक्त होते है। एक वृक्ष से तीन फसले ली जा सकती है। यूकेलिप्टस व पापलर का वर्तमान बाजार मूल्य 500-600 रूपयेध्कुन्टल है। 3. पैकिंग बाक्स उद्योग में यूकेलिप्टस, आम आदि की लकड़ी की बिक्री की जा सकती है। क्षेत्र की नजदीकी आरा मशीनों पर किसान वन विभाग से नियमानुसार कटान तथा दुलान परमिट प्राप्त कर वृक्षों की बिक्री कर सकते है। 4. इसके अतिरिक्त वन निगम द्वारा तैयार किये मानकों जैसे मोटाई के आधार पर देय मूल्य से भी कृषक प्रार्थना पत्र देकर वृक्षों की बिक्री कर सकते है। ग्रामीण विकास में कृषि वानिकी आम, नीम, कटहल, बबूल की प्रजातियाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में मांग के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उपलबध नहीं है। कुछ वर्षों बाद गावों में सागौन, शीशम, के पेड़ बहुत कम उम्र के होने के कारण काटे नही जा सकते है। जलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में लकड़ी उपलब्ध नही है जिससे जलौनी की समस्या उत्पन्न हो गयी है। आम के पेड़ जो लगभग 40 से 50 वर्ष पहले के थे, काटने के कारण बहुत कम रह गये है। भविष्य में इमारती लकड़ी तथा जलौनी की सतत उपलबधता हेतु योजनाबद्ध तरीके से इन महत्वपूर्ण प्रजातियों का रोपण राज्य वन विभाग, कृषकों तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाना चाहिए। आम (देशी आम), कटहल, नीम, बबूल बहुत कम उपलबध है, सागौन और शीशम पिछले कुछ वर्षों में लगाये है लेकिन देसी आम, कटहल, नीम को भी लगाने की जरूरत है जिससे इमारती लकड़ी और जलोनी पर्याप्त मात्रा में मिल सके। नये उम्र के आम (कलमी आम) से फल तो मिल रहा है लेकिन जलौनी के लिए लकड़ी नही मिलती है, इससे जलौनी की कमी हो रही है। गावों में यह पाया गया कि शीशम के 7 से 15वर्ष के पेड़ सूख जाते है। सागौन और शीशम पिछले कुछ वर्षों में लगाये है लेकिन देसी आम, कटहल तथानीम को भी लगाने की जरूरत है जिससे इमारती लकड़ी और जलौनी पर्याप्त मात्रा में मिल सके।
काष्ठ प्रजातियों के विक्रय के चरण
1. कृषक > ठेकेदार > कमीशन एजेंट > टिंबर ट्रेडर > अंतिम उपयोगकर्ता
2. कृषक > अंतिम उपयोगकर्ता
3. कृषक > ठेकेदार > टिंबर ट्रेडर
4. कृषक> ठेकेदार > अंतिम उपयोगकर्ता
5. कृषक> टिंबर ट्रेडर कार्पेटर अंतिम उपयोगकर्ता
6. कृषक > ठेकेदार > कमीशन एजेंट > अंतिम उपयोगकर्ता
7. कृषक> कमीशन एजेंट > अंतिम उपयोगकर्ता
8. वन निगम > ठेकेदार > टिंबर ट्रेडर > अंतिम उपयोगकर्ता
9. वन निगम > टिंबर ट्रेडर अंतिम उपयोगकर्ता
10. कृषक > ठेकेदार > टिंबर ट्रेडर अंतिम उपयोगकर्ता
11. कृषक > टिंबर ट्रेडर > अंतिम उपयोगकर्ता
प्रमुख काष्ठ प्रजातियों का विक्रय